श्याम बेनेगल धुंधलके से उठती बेआवाज़ों की आवाज़
श्याम बेनेगल अपनी फिल्मों में साहस के साथ हिंदुस्तान के स्याह- सच को
पूरी विश्वसनीयता और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। भारत को 'भूतो न भविष्यति' की तरह महिमामंडित करने वाले दर्शकों, आलोचकों ने आरंभ में श्याम बेनेगल को निशाने
पर इसलिए लिया कि उनकी फ़िल्में हिंदुस्तान के काला - स्याह पक्ष को ही उजागर करती
हैं। श्याम बेनेगल अपनी आलोचनाओं से कभी नहीं डिगे और प्रत्येक साल कोई न कोई
फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाते रहे। उनका कहना यही था कि मैं सिर्फ सच दिखलाता हूं।
अगर अधिकांश हिंदुस्तानियों के हिस्से का सच 'काला' है
तो मैं उसे श्वेत- सफेद कैसे दिखला सकता हूं? चहुं ओर जब जुल्म हो, शोषण हो, पस्ती
और जहालत हो तो फिर किस प्रकार कोई सच्चा और दायित्वपूर्ण फिल्म निर्देशक आंखें
चौंधियाने वाली ' चकाचक'
फिल्में बना सकता है? बेनेगल की फिल्म निर्माण के दर्शन और मिजाज को हम नागार्जुन
की इन पंक्तियों से समझ सकते हैं -
तुम ही बताओ मीत कि कैसे अमरित बरसाऊं
कहो कि कैसे झूठ बोलना सीखू और सिखलाऊं
कहो कि अच्छा ही अच्छा सब कुछ कैसे दिखलाऊं
कहो कि कैसे सरकंडे से स्वर्ण किरण लिख पाऊं
श्याम बेनेगल के समय भी मुख्य धारा के अधिकांश निर्माता- निर्देशक अपनी
फिल्मों के माध्यम से झूठ बोलना 'सीख' और 'सिखा' रहे थे और आज तो 'सरकंडे से स्वर्ण किरण लिखने' वाले निर्देशकों की पूरी फौज खड़ी है।
लेकिन श्याम बेनेगल को यह मंजूर नहीं था। इसलिए वे श्याम बेनेगल थे।
श्याम बेनेगल की पहचान सिर्फ़ एक सरोकार सम्पन्न निर्देशक की ही नहीं रही
है,
वे एक बुद्धिजीवी और सचेत नागरिक भी रहे हैं।
कठिन समय में जोखिम उठाकर अपने लेखनों, भाषणों और साक्षात्कारों में सत्ता की तीखी आलोचना करना वे
नागरिक - दायित्व समझते थे। जुलाई 2019 में जिन 49 लोगों
ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा था उनमें श्याम बेनेगल प्रमुख थे। चिट्ठी में देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं
पर चिंता व्यक्त की गई
थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कड़ा कदम उठाने की मांग की गई थी। पत्र में
अल्पसंख्यकों और दलित समुदाय के लोगों के साथ हुई लिंचिंग की घटनाओं के आंकड़े भी
पेश किए गए थे। प्रधानमंत्री के नाम इस खुले खत में देश के नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों
का भी हवाला दिया गया था। इसी पत्र के कारण श्याम बेनेगल पर राजद्रोह का एफआईआर भी दर्ज़ हुआ था। आशय यह कि वे सेफ
जोन में रहकर फिल्म बनाकर संतुष्ट रहनेवाले फिल्मकार नहीं थे।
अंकुर, निशांत, मंथन
और आरोहण आदि फिल्में भारतीय गांव की सच्चाई से हमारा साक्षात्कार कराती है। 1960-70 के दशक
के हिंदुस्तान का सहमता गांव इन फिल्मों में सजीव हो उठा है। गांव की सामंती
व्यवस्था,
इस व्यवस्था का अमानवीय चेहरा और दमन के क्रूरतम रूप
को कैमरे ने विलक्षण रचनात्मकता के साथ कैद किया है। श्याम बेनेगल ने पहली
फिल्म 'अंकुर' में ही अपने निर्देशन क्षमता की धाख जमा ली थी। उन्हें अपनी
इस पहली फिल्म पर ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया था। यह फिल्म हमें चुपके से यह कह
जाती है कि जमींदार की दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी की अपेक्षा अधिक क्रूर, धूर्त और कायर है। पहली पीढ़ी का जमींदार अपने रखैल को सबसे
अच्छी जमीन देता है और उसके बेटे को सार्वजनिक रूप से अपना पुत्रवत घोषित करता है।
उसके परिवार का लालन- पालन का दायित्व उठता है। उसी जमींदार का पुत्र सूर्या (अनंतनाग)
ऊपर से जितना ही मीठा- मधुर दिखता है भीतर से उतना ही क्रूर
और धूर्त है। वह एक मूक- बधिर दलित खेत मजदूर किस्तैया को अपमानित कर गांव छोड़ने पर विवश करता
है। उसकी गिद्धदृष्टि उस दलित मजदूर की युवा पत्नी लक्ष्मी (शबाना आजमी) पर लगी
हुई है। वह उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लेता है। किंतु पत्नी के आते ही उसे
दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देता है। उस स्त्री के गर्भ में पल रहे अपने
बच्चे को निर्दयता पूर्वक हटाने को कहता है और उसे भी गांव छोड़ने का निर्देश देता
है। लेकिन लक्ष्मी उस बच्चे जन्म देने पर तुली हुई है। वह
साहसपूर्वक कायर प्रेमी का प्रतिवाद करती है। किस्तैया के लौट
आने पर वह अपने गुर्गों से अनावश्यक
रूप से उसकी पिटाई करवाता है। उसे डर है कि कहीं वह गर्भ का सत्य जान जाएगा तो पूरे गांव को यह रहस्य उद्घाटित कर देगा। दूसरी तरफ़
यह जानते हुए कि गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है वह मूक
बधिर दलित मजदूर
पत्नी की मनोवांछित इच्छा की पूर्ति होने की संभावना मात्र से आह्लादित होता है।
किस्तैया को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है? चूंकि वह पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है इसलिए उसकी खुशी
में वह अपनी खुशी ढूंढता है। लक्ष्मी के प्रति सूर्या और किस्तैया के प्रेम का
फ़र्क
वर्गीय प्रेम का फ़र्क है। सामंत सूर्या के लिए प्रेम का
मतलब भोग और प्रेम का प्रदर्शन है लेकिन किस्तैया के लिए प्रेम जीने - मरने का सवाल है। वह बार बार अपमानित
होता है,
पिटता है लेकिन लक्ष्मी के दिल से हटता नहीं है।
सूर्या के बार-बार यह कहने पर कि किस्तैया शराबी है, चोर है, निकम्मा
है;
लक्ष्मी भी बार - बार कहती है 'नहीं साहेब, वह बहुत अच्छा आदमी है'। किस्तैया की पिटाई के प्रतिकार में लक्ष्मी जिस प्रकार से
सूर्या को फटकार लगाती है उससे उसके दृढ़ चरित्र का पता चलता है। सामंती व्यवस्था
में स्त्री की दुर्दशा और दुर्गति को 'अंकुर' फिल्म
बेनकाब करती है। पत्नी
को ज़रखरीद गुलाम समझना, उसे जुए
में दाव पर लगाना इस सामंती व्यवस्था की शान है। पंचायत भी स्त्री को अनसुना कर
देता है। पति और परंपरा ही सामंती व्यवस्था (पंचायत )की मुख्य आवाज बन जाती है।
फिल्म
'निशांत' में
कथा नायक स्कूल मास्टर ( गिरीश कर्नाड) अपनी जवान पत्नी ( शबाना आज़मी) को अगवा
करनेवाले ताकतवर जमींदार के खिलाफ़ गांव के लोगों को एकजुट करता है। यह फिल्म यह दिखाने में सफल रही है कि
भारतीय गाँव में ताकतवर वर्चस्वशाली जमींदार के सामने
किस तरह आम जन से लेकर सरकारी मिशनरी तक लाचार हो जाते हैं। सबकी आंखों के सामने स्त्री को उठाकर ले जाया जाता है, लेकिन जमींदार के ख़ौफ के कारण कोई चूं तक नहीं कर पाता।
पुलिस भी जमींदार के पाले में। उस स्त्री का बार - बार बलात्कार होता है लेकिन
लोकतंत्र का कोई पाया
एक स्त्री को बचा नहीं पाता।
कथानक
और निर्देशन का कमाल यह है कि
लोकतंत्र के पाये की इस असमर्थता और कायरता के प्रतिकार में कथानायिका अपहरण करने
वाले के साथ हो जाती है। बावजूद इसके कि सामूहिक बलात्कार जनित अपमान के
विनाशकारी अनुभवों से वह गुजर चुकी होती है। वह बाद में
क्रूर वास्तविकता को स्वीकार कर लेती है और अपहृत घर में आराम से रहती है। अंततः
वह विश्वम ( जिसके लिए उसका अपहरण किया गया था) की ओर आकर्षित होने लगती है। उसकी
अनुपस्थिति उसके पति को पीड़ा देती है और उसकी लाचारी उसके जीवन को दुखी बनाती है।
सिनेमा का सबसे बेहतरीन दृश्यों में से एक वह है जब वे (पति - पत्नी) आखिरकार एक
स्थानीय मंदिर में मिलते
हैं। वह पति को उसकी कायरता के लिए लताड़ती है। यह फिल्म जमींदारों- सामंतों की
अपेक्षा आम जन में बदलाव और आंतरिक शक्ति संचय की कलात्मक मांग करती है। फिल्म के अंत में सुरंग में
प्रकाश- किरण का दिखना उम्मीद के बचे रहने का संकेत है।
'मंथन' फिल्म की खूबी यह है कि यह किसानों द्वारा किसानों के लिए
बनाई गई फिल्म है। इसके महत्त्व को हम इस तथ्य से आंक सकते हैं
कि इसके निर्माण में पांच लाख किसानों ने दो
- दो रुपए चंदे दिए थे। किसान ट्रकों पर
लदकर फिल्म देखने आते थे। 'मंथन' दूध उत्पादक किसान - मजदूरों के आर्थिक शोषण और हक की सच्ची (अंशत:) लड़ाई का सिने
रूपांतरण है। मंथन में गुजरात के दूध उत्पादक किसानों को बिचौलियों के चंगुल से
बचाने के लिए एक युवा पशु चिकित्सक डॉ मनोहर राव (गिरीश कर्नाड ) कोऑपरेटिव डेयरी
की स्थापना करता है, जिसका
स्वामित्व और प्रबंधन ग्रामीणों द्वारा स्वयं किया जाना है। डॉ राव और उनकी टीम को
गाँव की राजनीति, कठोर
जातिवाद और गाँव के लोगों के प्रति सामान्य अविश्वास से जूझना पड़ता है। बहुत
मशक्कत के बाद इन्हें स्थानीय हरिजन समुदाय के नेता भोला (नशरुद्दीन शाह)
का साथ मिल पाता है। गांव की बिंदु (स्मिता पाटिल) महिलाओं को संगठित करती है। गांव पर मिश्रा जी
(अमरीश पुरी) का दबदबा है, वे औने -
पौने भाव में किसानों से दूध लेते हैं। फिल्म में राव की टीम और भोला का मिश्रा के
साथ संघर्ष को
सिलसिलेवार ढंग से दिखाया गया है। गांव की राजनीति फिल्म के केंद्र में है।
इन फिल्मों में सामंती व्यवस्था के प्रति आक्रोश और सामाजिक बदलाव के लिए जद्दोजेहद करते मध्य वर्ग और कामगारों की भूमिका को साफ देखा जा सकता है। फिल्म अंकुर के अंत में एक बच्चे को जमींदार के घर पर पत्थर फेंकते हुए दिखाना उस प्रतिरोधी तेवर को दर्शाता है जो धीरे-धीरे कलात्मक हिंदी फिल्मों के लिए अनिवार्य होता चला गया। अंकुर के बाद श्याम बेनेगल अपनी फिल्मों विशेषकर निशांत, मंथन और आरोहण में अधिक गतिशील होते हैं। (कु) व्यवस्था के प्रति असहमति और क्रोध अधिक मुखर होकर इन फिल्मों में सामने आता है।
सत्यजीत
राय (अछूत कन्या) के साथ श्यामबेनेगल
(अंकुर,
मंथन, आरोहण)
ऐसे
चंद फिल्मकारों में हैं जो हिंदुस्तान की वर्णव्यवस्था को
आलोचना और बहस को केंद्र में लाते हैं।
दलित पात्र को रजतपट पर ससम्मान उतारना, उनके दुखों और पीड़ाओं को जगजाहिर करना और वर्णव्यवस्था की
क्रूरता और अमानुषिक
व्यवहार को दिखाने का सामाजिक ही नहीं व्यावसायिक जोखिम भी वे उठाते हैं।
फिल्म आरोहण ( 1982) में श्याम बेनेगल का वाम रुझान बहुत स्पष्ट है। फिल्म बोरगादार (जमीन जीतनेवाला) और जोतदार (जमीन का मालिक) के बीच भीषण संघर्ष को दिखाता है। बोरगादार श्रमिकों के संघर्ष और उनकी पस्ती को दिखाने में श्याम बेनेगल सफल रहे हैं। कथा हरिमंडल ( ओम पुरी ) नाम के एक गरीब किसान की है जो अपनी पत्नी, दो बेटों, भाई, एक बूढ़ी विधवा चाची कालीदाशी ( गीता सेन ) और उसकी बेटी पंची के साथ बीरभूम जिले के गिरिपुर के सुदूर बंगाल गांव में रहता है । फिल्म की कहानी साठ के दशक के मध्य में शुरू होती है "जब नक्सलबाड़ी विद्रोह पूरे बंगाल में फैल रहा था और उत्पीड़ित किसानों को साम्यवाद और समाजवादी गणराज्य में विश्वास रखने वाले युवाओं द्वारा एकजुट किया जा रहा था।" फिल्म के केंद्र में कोलकाता और उसके गांव हैं। वर्ग संघर्ष और वर्ण संघर्ष की संपृक्ति सिनेमा को समग्रता प्रदान करती है।
वाडेकर
के जीवन में एक तरफ़ उपलब्धियां
थीं,
शोहरत थी तो दूसरी तरफ़ लांछना। इस विडंबनात्मक परिस्थिति
ने उसे न सिर्फ़ शराबी बना दिया बल्कि दो - दो बार आत्महत्या के लिए विवश भी किया। विशेषकर
एक स्त्री के लिए फिल्म को एक चुनौतीपूर्ण माध्यम के रूप पेश किया गया है। अमोल
पालेकर,
अनंत नाग, नसरुद्दीन
शाह,
अमरीश पुरी जैसे सधे अभिनेताओं ने फिल्म को एक अलग मयार
दिया है।
श्याम
बेनेगल की फिल्में गांव की पृष्ठभूमि की हो या नगर की, एक विशेष प्रकार की चेतना का साक्षात्कार दर्शकों को होता
है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बाद उन्होंने महानगर की ओर रुख किया। जुनून(1978),
कलियुग (1981), मंडी (1983), त्रिकाल (1985) सरीखी फिल्में शहरी जीवन की जटिलता, विषमता और मानसिकता को उद्घाटित करती हैं।
इन फिल्मों में विषयगत विविधता और प्रस्तुति की नवीनता ने
गंभीर फिल्म समीक्षकों को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित किया। ग्रामीण पृष्ठभूमि
की फिल्मों की अपेक्षा ये फिल्में जटिल और आंशिक रूप से
दुर्बोध हैं। जिस प्रकार ग्रामीण जीवन सरल होता है, नागर-जीवन उतना सरल-सहज नहीं होता। स्वभावतः इन फिल्मों की कई परतें हैं। सभी परतें एक - दूसरे
से गूंथे और उलझे हुए हैं। इसी गुत्थमगुत्था में फिल्म की सार्थकता है। इसलिए इन फिल्मों को सजग और
साकांक्ष होकर देखना पड़ता है। 'जुनून' की पृष्ठभूमि 1857 का गदर है। यह फिल्म रस्किन बांड के उपन्यास 'ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स' पर आधारित है। फिल्म में इस महाविद्रोह को यथार्थ और
विलक्षण सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उस समय के हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की मानसिक बुनावट और अंतर्द्वंद्व की पड़ताल
फिल्म को विशिष्ट बनती है। फिल्म में एक कश्मकश भरी प्रेमकथा है। मुसलमान जावेद और
ईसाई रूथ एक दूसरे को
बेइंतहा चाहते हैं। पारंपरिक- धार्मिक दूरी और राजनीतिक रूप से दुश्मनी इन दोनों
के प्रेम में पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती है। फिल्म यह दिखाती
है कि धार्मिक और राजनीतिक दूरी विवाह पर तो पाबंदी लगा
सकती है,
प्रेम पर नहीं। फिल्म के अंत में जावेद 1857 के महासंग्राम में मारा जाता है और रूथ इंग्लैंड चली जाती
है।
फिल्म
'कलियुग' नितांत भिन्न धरातल की फिल्म है। यह आधुनिक महाभारत है। यह
प्राचीन महाभारत का आधुनिक संस्करण और नए संदर्भों में महाभारत का पुनर्कथन। गुजरा ज़माना राजा -
महाराजाओं का था। उनका अंतर्कलह, संघर्ष, चतुराई और छल से हम सभी परिचित हैं। यह ज़माना उद्योग और
व्यवसाय का है तो श्याम
बेनेगल ने 'कलियुग' में एक बड़े व्यावसाई परिवार के अंतर्कलह, उठा - पाठक, दाव - पेंच और षड्यंत्रपूर्ण हत्या को दिखलाया है। कथानक ही
नहीं चरित्रों के नाम भी महाभारत- प्रेरित हैं। करण की भूमिका में शशिकपूर ने
अदभुत रूप से सिने समीक्षकों और दर्शकों को प्रभावित किया था। इस किरदार से शशि
कपूर अभिनय के नए 'अवतार' के रूप में सामने आए थे।
'त्रिकाल' बेनेगल द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म है, जो
पुर्तगाली शासन के अंतिम समय के दौरान गोवा में घटित हुई थी। फिल्म की कथा उस समय की है जब 1961 में भारतीय सेना ने गोआ को कॉलोनी मुक्त करवाया था। फिल्म का अधिकांश
हिस्सा फ़्लैशबैक शैली में कही गई है। ईसाई परिवार की जद्दोजेहद, प्रेम, विवाह, अंधविश्वास आदि इस फिल्म की रीढ़ है। ईसाई समाज में भी
अंधविश्वास की गहरी जड़ें हैं। कथा नायक रूईज परेरा (नशरुद्दीन शाह ) लंबे अर्से
बाद घर लौटता है। तबतक घर खंडहर में तब्दील हो चुका होता है। घर ही नहीं रूईज का
दिल भी खंडहर हो चुका है। फिल्म के अंत में कथा नायक का लंबा एकालाप फिल्म के
विलक्षण दृश्यों में एक है। परिस्थितियों और चरित्रों जिसमें वह ख़ुद भी शामिल है
की निर्मम आलोचना इस एकालाप को महत्वपूर्ण बनाती है।
वेश्याओं के जीवन पर बनी कुछ बेहतरीन फिल्मों में एक है - मंडी। यह फिल्म उर्दू के एक बड़े लेखक गुलाम अब्बास की क्लासिक कथा 'आनंदी' पर आधारित है। यह फिल्म जहां एक ओर वेश्या जीवन की घुटन और त्रासदी को दिखाती है वहीं उसके प्रभाव और रसूख को भी। वेश्यावृत्ति और राजनीति का अद्भुत गठजोड़ फिल्म की खासियत है। विषम और जटिल परिस्थितियों में प्रेम की कोंपले खिलाना बेनेगल के निर्देशन की निजी विशेषता रही है। फिल्म में अत्यंत प्रतिष्ठित व्यापारी (सईद जाफरी) पुत्र सुशील (आदित्य भट्टाचार्य ) जीनत (स्मिता पाटिल) नामक नर्तकी वेश्या से प्रेम कर बैठता है। दोनों का प्रेम परवान चढ़ता है, तभी ज्ञात होता है वे दोनों भाई - बहन हैं। दरअसल जीनत सुशील के पिता मिस्टर अग्रवाल की नाजायज़ संतान है। उसका जन्म किसी वेश्या के गर्भ से हुआ था और लालन - पालन मशहूर वेश्या रुक्मिणी बाई (शबाना आज़मी) ने किया था। मिस्टर अग्रवाल की प्रतिष्ठा दाव पर न लगे, रुक्मिणी इसे छिपाए रखती है। इस प्रेम से नाखुश रुक्मिणी जीनत को सच्चाई बता देती है। अपराधबोध में जीनत अपने को सुशील से दूर कर लेती है और एकाकी जीवन जीने पर विवश होती है।
'वेलकम टू सज्जनपुर' बेनेगल की अंतिम फीचर (व्यायसायिक) फिल्म है। इसको
विद्रूपताओं के बीच सुखांत की तलाश की फिल्म कह सकते हैं। स्वयं बेनेगल ने इसे 'ब्लैक कॉमेडी' की संज्ञा दी थी। हिजड़ों की समस्याओं, सरोकारों और उनकी अथाह संवेदनशीलता को यह फिल्म उद्घाटित
करती है। हिजड़ों के माध्यम से जिस त्रासद से बेनेगल हमें रूबरू
करवाते हैं, वह अत्यंत कारुणिक और
अवसादजनक है। इस फिल्म को एक और कारण से याद किया जाना चाहिए। निर्देशक ने सायास
नायक और नायिका के नाम में निम्न जाति सूचक टाइटिल लगाया है
- महादेव कुशवाहा और कमला कुम्हारिन।
जिस 'देस' में निम्न वर्णीय टाइटिल देखकर ही ' कुछ कुछ होने लगता' है वहां हीरो और हीरोइन के नाम में कुशवाहा और कुम्हारिन
लगाना साहस का काम है। बावजूद फिल्म को लोगों ने पसंद किया था।
जातिगत विद्वेष और वंचना के अतिरिक्त यह फिल्म हिजड़ों के
प्रति सामाज में आए बदलाव को भी रेखांकित करती है। मध्यप्रदेश में किन्नर शबनम का
भारी मतों से विधान
सभा का चुनाव जीतना एक सामाजिक
संकेत है। इस संकेत के माध्यम से बेनेगल यह दिखाना चाहते थे कि तथाकथित अच्छे
नेताओं से लोगों का मोहभंग हुआ है। जिस प्रकार 'राजनीति का अपराधीकरण' और 'अपराध का
राजनीतीकरण' हुआ है लोग हिजड़ा
मुन्नी में संभावना तलाशने लगे हैं। दूसरी तरफ़ यह फिल्म यह भी बताती है कि जिस
हिजड़ा को समाज छक्का, वेश्या, निर्लज्ज कहकर अपमानित करता है, वह भी आखिर इंसान है और संभावनाओं से संपन्न भी। फिल्म में
मुन्नी बाई अपने जैविक और पारंपरिक स्वभाव के साथ अद्भुत गंभीरता और संवेदनशीलता
का परिचय देती है। मुन्नी का किरदार ऐसे लोगों पर तमाचा है जो हिजड़ों को
हेय, अयोग्य
और घृणित समझते हैं। निर्देशक ने मात्र दो पत्रों के हवाले से परस्पर दो विरोधी स्थितियों
को उजागर किया है। एक पत्र राजनीति को अपनी 'लुगाई' समझने
वाले यशपाल शर्मा का है। वह अंगूठा छाप है किंतु अपने नेतागिरी के गुमान में
स्थानीय डी एम को दो कौड़ी का समझता है। अत्यंत अभद्र भाषा में पत्र लिखकर हिजड़ा
मुन्नी बाई का चुनाव रद्द करने का फ़रमान जारी करता है। क्योंक उसकी नज़र
में 'एक
हिजड़ा चुनाव जीतकर पूरे गांव को हिजड़ा बना देगा'। ठीक इसके विपरीत उस नेता की दादागिरी से तंग आकर मुन्नी
भी डी एम को पत्र लिखती है। मुन्नी का पत्र समाज में
प्रचलित हिजड़ों के प्रति बद्धमूल धारणा को ध्वस्त करता है
- "डीम साहब, हम
हिजड़े भी इंसान होते हैं । ये लोग हमें ऐसे धमका रहे हैं जैसे हम रावण हैं। क्या
हमको दुख नहीं होता? हमसे लोग
क्यों नफ़रत करते हैं? क्या हम
इंसान नहीं हैं?...
आपकी
और सबकी
मुन्नीबाई
इस
पत्र की विशेषता यह है कि यह सामान्य पत्र न रहकर हिजड़ों को मनुष्य का दर्ज़ा दिए
जाने का माँगपत्र बन जाता है। इस फिल्म में इसके अतिरिक्त पत्र लेखन के विलोपन
की विडंबना तथा समाज में अंधविश्वास की निरंतर घुसपैठ को भी
रोचकता से रेखांकित किया गया है।
श्याम
बेनेगल ने लगभग दो दर्जन फिल्में बनाई हैं, जिनपर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक - दो किताबें भी कम
पड़ेंगी। उनकी कुछ अन्य बेहतरीन फिल्मों हैं सुषमन, यात्रा, अंतर्नाद, सूरज का सातवां घोड़ा, सरदारी बेगम, जुबेदा, ममो, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आदि। बेनेगल के निर्देशन की तकनीक, प्रस्तुति के तरीके, कथा-कहानी का फिल्मी रूपांतरण, कैमरे
की गतिविधि, प्रकाश का धुंधलका, गीत - संगीत के साथ पार्श्व संगीत का वैशिष्ट्य, परिधान की विश्वसनीयता आदि विषयों पर भी अलग - अलग किताबें
लिखी जा सकती हैं। उनको और उनके साथ काम करने वाले अभिनेताओं और सहयोगियों को मिले
कई पुरस्कार और सम्मान पर भी किताब लिखी जा सकती है। उन्होंने जितनी भी फिल्में
बनाईं लगभग सभी पुरस्कृत और सम्मानित हुईं। दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह
में उनकी फ़िल्में दिखाईं गईं।उन्हें अठारह बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से
सम्मानित किया गया। वे पुरस्कार विजेता निर्देशक के रूप में भी जाने जाते हैं।
'भारत एक खोज' की चर्चा के बगैर श्याम बेनेगल पर चर्चा संभव नहीं है। वे 'भारत एक खोज' के पर्याय बन गए हैं। दुनिया भर के मशहूर और प्रतिष्ठित
धारावाहिकों में 'भारत एक
खोज'
का शुमार है। धारावाहिक दुनिया में उन्होंने ऐसी मयार खींच दी है, जिसे पाट पाना मुश्किल है। उन्होंने एक बेहतरीन इतिहास (जवाहरलाल नेहरू)
को जन इतिहास बना दिया। उन्होंने
कुल तिरेपन एपिसोड में भारत के पांच हजार साल (1947 तक) के इतिहास को आम भारतीयों के जेहन में उतार दिया। आज
जिस तरह से इतिहास के नाम पर मिथ और मिथ्या को परोसा जा रहा है, हम 'भारत एक
खोज'
धारावाहिक देखकर अपना इतिहासबोध बना सकते हैं। विभाजनकारी
इतिहास के समानांतर 'भारत एक
खोज'
हमें सामासिक और समन्वयकारी इतिहास चेतना से लैस करता है। श्याम बेनेगल/शाम जैदी की पटकथा, वी के मूर्ति का छायांकन और ओमपुरी, रोशन सेठ, टॉम
ऑल्टर,
सदाशिव अमारवपुरकर आदि की सशक्त भूमिका ने भारत एक खोज को
चिर स्मरणीय धारावाहिक के रूप में स्थापित कर दिया। 23 दिसंबर, 2024 को वे दिवंगत हो गए। उनके बेमिसाल, प्रेरक फिल्मी सफर और उनके साहसी नागरिक-बोध को सलाम।
|
|
|
|||
|
||||
।














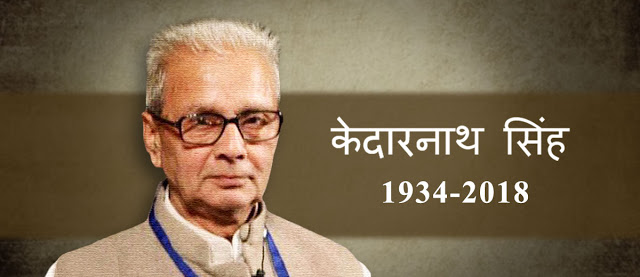
Comments
Post a Comment